MSP का गणित टूटा ?
2025 में कानूनी गारंटी के बिना किसानों के विकल्प

परिचय
भारत की कृषि व्यवस्था में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह स्तंभ रहा है जिसने दशकों से किसानों को बाजार की अनिश्चितताओं से बचाने का काम किया है। MSP एक सरकारी गारंटी-प्राइस है जो किसान को उसकी फसल का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करता है, भले ही बाजार में कीमत गिर जाए। इसे किसानों के लिए “सुरक्षा-कवच” कहा गया क्योंकि यह उन्हें घाटे में बेचने के जोखिम से बचाता था।
1950–60 के दशक में हरित क्रांति के समय, MSP ने गेहूं और धान के उत्पादन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरकार ने किसानों से अनाज खरीद कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को मजबूत किया। इसके कारण देश ने खाद्यान्न सुरक्षा पाई और आयात निर्भरता कम की। किसानों के लिए यह व्यवस्था एक भरोसेमंद सहारा थी – अगर बाजार में व्यापारी भाव गिरा दें, तो भी सरकार तय कीमत पर खरीदारी करेगी।
लेकिन जैसे-जैसे दशक बीते, MSP व्यवस्था कई समस्याओं से घिर गई। यह केवल कुछ फसलों और कुछ राज्यों तक सीमित रह गई। सरकारी खरीदारी केंद्र उत्तर भारत के कुछ राज्यों जैसे पंजाब और हरियाणा में केंद्रित हो गए। बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश जैसे राज्यों के किसान मंडी व्यवस्था और सरकारी खरीदारी के अभाव में MSP का फायदा नहीं उठा सके।
आज 2025 में हालात और भी पेचीदा हैं। किसानों की बड़ी आबादी—लगभग 86% छोटे और सीमांत किसान—MSP से लाभान्वित नहीं हो पाते। सरकारी खरीदारी सीमित है। प्राइवेट व्यापारी अक्सर MSP से कम दाम पर खरीदते हैं। सरकारी गोदामों में जगह की कमी और FCI (भारतीय खाद्य निगम) की वित्तीय स्थिति ने भी खरीद सीमाओं को बाधित किया है।
एक और बड़ा सवाल MSP की कानूनी गारंटी का है। 2020–21 के किसान आंदोलन के दौरान MSP को कानूनी गारंटी देने की मांग बहुत जोर पकड़ गई थी। किसान संगठनों ने कहा कि सिर्फ घोषणा काफी नहीं—कानूनी मजबूरी होनी चाहिए कि कोई भी व्यापारी MSP से कम दाम पर न खरीदे। मगर सरकार ने तर्क दिया कि कानूनी गारंटी व्यवहारिक नहीं है – इससे सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा, बाजार विकृत होगा और प्राइवेट सेक्टर बाहर निकल सकता है।
किसानों के लिए यह एक कड़वी सच्चाई है कि 2025 में न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई कानूनी गारंटी नहीं है। गेहूं या धान के लिए सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना भी उचित क्यों न हो, अगर वह सरकारी खरीद केंद्रों तक नहीं पहुंचता या खरीद सीमित है, तो किसान को मजबूरी में कम दाम पर बेचना पड़ता है। यह केवल आंकड़ों का खेल बनकर रह जाता है।
इसका नतीजा यह है कि MSP को लेकर किसानों में अविश्वास बढ़ा है। कुछ किसान इसे सरकार का “जुमला” मानते हैं, तो कुछ इसे उत्तर भारत केंद्रित नीतिगत भेदभाव कहते हैं। किसानों के असली सवाल हैं – “क्या मेरी फसल MSP पर बिकेगी?” और “अगर नहीं बिकेगी तो मैं क्या करूं?”
इन सवालों ने एक बड़ी बहस को जन्म दिया है:
● क्या MSP व्यवस्था फेल हो रही है?
● क्या MSP सिर्फ आंकड़े हैं या जमीन पर किसानों की गारंटी?
● MSP की कानूनी गारंटी के बिना किसान कैसे टिक पाएंगे?
● किसानों को क्या विकल्प तलाशने चाहिए?
आज इन गंभीर मुद्दों पर ईमानदार और व्यावहारिक चर्चा की सख्त जरूरत है। किसानों को सिर्फ भावनात्मक घोषणाओं की नहीं, बल्कि ठोस विकल्पों की सख्त जरूरत है।
सामग्री की तालिका
MSP क्या है और क्यों बना ?
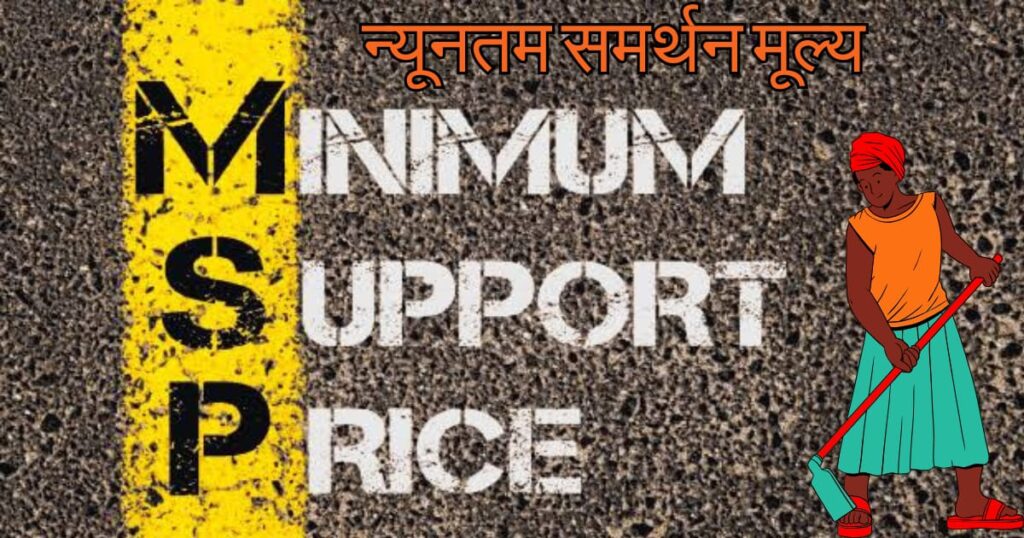
भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां करीब 50% आबादी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। मगर कृषि हमेशा से ही जोखिमों से भरी रही है—मौसम की मार, बाजार की अनिश्चितता और दाम गिरने का डर किसानों की सबसे बड़ी समस्याएं रही हैं।
इन समस्याओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की अवधारणा एक उपयुक्त समाधान के रूप में उभरी। न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार द्वारा किसानों को उनकी कृषि उपज के लिए दी जाने वाली न्यूनतम कीमत है। जो सरकार किसानों को उनकी उपज के लिए देने की गारंटी देती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बाजार में फसल के दाम MSP से नीचे चले जाएं, तो भी सरकार तय कीमत पर किसानों की फसल खरीदेगी।
MSP की शुरुआत क्यों हुई?
MSP की नींव हरित क्रांति के समय पड़ी। 1960 के दशक में भारत में भयंकर खाद्यान्न संकट था और देश गेहूं-चावल विदेशों से आयात करने को मजबूर था। किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित करना जरूरी था। मगर किसान तभी ज्यादा उत्पादन करेंगे जब उन्हें अपनी उपज का उचित दाम और बिक्री की गारंटी हो।
तब सरकार ने कहा – “आप उगाइए, हम न्यूनतम कीमत की गारंटी देंगे।” यही MSP की मूल भावना थी। सरकार ने गेहूं और धान जैसी प्रमुख फसलों के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया और बड़ी मात्रा में सरकारी खरीदारी शुरू की।
MSP की शुरुआत क्यों हुई?
भारत सरकार हर साल खरीफ और रबी सीजन की 23 प्रमुख फसलों के लिए MSP तय करती है। ये फसलें हैं:
खरीफ की फसलें (14 फसलें):
- 1 धान (Paddy)
- 2 ज्वार (Jowar)
- 3 बाजरा (Bajra)
- 4 मक्का (Maize)
- 5 मूंगफली (Groundnut)
- 6 सोयाबीन (Soybean)
- 7 सूरजमुखी (Sunflower seed)
- 8 तिल (Sesame)
- 9 अरहर (Tur/Red Gram)
- 0 उड़द (Urad)
- 11 मूंग (Moong)
- 12 कपास (Cotton)
- 13 रामी (Nigerseed)
- 14 गन्ना (Fair and Remunerative Price याने कीं लाभकारी मूल्य घोषित होता है, MSP जैसा ही माना जाता है)
रबी की फसलें (6 फसलें):
- 15 गेहूं (Wheat)
- 16 जौ (Barley)
- 17 चना (Gram)
- 18 मसूर (Lentil)
- 19 सरसों (Rapeseed/Mustard)
- 20 कुसुम (Safflower)
वाणिज्यिक फसलें (3 फसलें):
- 21 कपास (Cotton) (खरीफ में गिना जाता है, पर यह महत्वपूर्ण नकदी फसल है)
- 22 जूट (Jute)
- 23 गन्ना (Sugarcane – FRP घोषित
MSP की सिफारिश CACP (Commission for Agricultural Costs and Prices) कृषि लागत और मूल्य आयोग नाम की संस्था करती है। यह आयोग किसानों की लागत, बाजार के दाम, अंतरराष्ट्रीय भाव, किसी वस्तु या सेवा की मांग और उपलब्धता के बीच संबंध जैसे तमाम फैक्टर्स का विश्लेषण करता है और फिर केंद्र सरकार को सलाह देता है।
MSP के मुख्य उद्देश्य
किसानों को न्यूनतम कीमत का भरोसा देना
MSP किसानों को आश्वासन देता है कि उनका माल औने-पौने दामों पर नहीं बिकेगा। यह “फ्लोर प्राइस” की तरह है – एक न्यूनतम स्तर जिसके नीचे कीमत नहीं जानी चाहिए।
कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना
MSP ने विशेषकर गेहूं और धान उत्पादन को बहुत अधिक तेजीसे बढ़ाया। किसानों को पता था कि अगर वे इन फसलों को उगाएंगे तो सरकार खरीद लेगी। इससे खाद्यान्न आत्मनिर्भरता आई।
बाजार की अस्थिरता से सुरक्षा देना
कृषि बाजार में कीमतें अक्सर गिरती-बढ़ती रहती हैं। अगर अच्छी पैदावार के चलते सप्लाई ज्यादा हो जाए तो दाम गिर जाते हैं। MSP किसानों को इस उतार-चढ़ाव से सुरक्षा देता है।
MSP का महत्त्व:
- यह खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- गरीबों को PDS (सार्वजनिक वितरण व्यवस्था) के जरिए सस्ता अनाज मिलता है।
- किसानों की आय में स्थिरता आती है।
- सरकार फसल विविधीकरण के लिए भी MSP घोषित करती है ताकि सिर्फ गेहूं-धान पर निर्भरता न रहे।
एक उदाहरण
मान लीजिए सरकार ने गेहूं का MSP रु. 2275/क्विंटल घोषित किया है। अगर मंडी में व्यापारी रु.1800 देने को तैयार हो तो किसान सरकार के खरीद केंद्र पर जाकर रु. 2275 में बेच सकता है। इससे किसान को नुकसान नहीं होता।
सरकारी भूमिका
सरकार MSP के जरिए सिर्फ घोषणा नहीं करती, बल्कि बड़े पैमाने पर फसल खरीदती भी है। FCI (भारतीय खाद्य निगम) और राज्य एजेंसियां किसानों से सीधे खरीदारी करती हैं और अनाज का भंडारण करती हैं।
निष्कर्ष
MSP भारतीय कृषि व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। इसका मकसद सिर्फ किसानों को कीमत देना नहीं, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना भी है। यह किसानों को आत्मविश्वास देता है कि वे जोखिम लेकर उत्पादन बढ़ा सकें।
MSP का गणित कैसे टूट रहा है?

भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की विचारशील धारणा किसानों को बाजार की अस्थिरता से बचाने के लिए लाई गई थी। सरकार हर साल 23 फसलों के लिए MSP घोषित करती है और कहती है – “इससे कम में मत बेचो, हम खरीद लेंगे।”
लेकिन 2025 में जमीनी सच्चाई यह है कि MSP अब सिर्फ सरकारी कागजों और घोषणाओं में ही जिंदा है। करोड़ों किसानों के लिए यह कोई ठोस सुरक्षा नहीं बन पाया। MSP के गणित में कई ऐसी खामियां हैं जिन्होंने इसे असली कवच बनने से रोक दिया।
1. खरीदारी सिर्फ चुनिंदा राज्यों तक सीमित
MSP का सबसे बड़ा संकट यह है कि सरकारी खरीदारी कुछ गिने-चुने राज्यों में ही होती है।
उदाहरण के लिए:
- भारत सरकार खरीदारी कुछ गिने-चुने राज्यों में मतलब पंजाब और हरियाणा से 70-80% गेहूं और चावल खरीदती है।
- इन राज्यों में खरीदारी केंद्र, मंडी सिस्टम और FCI गोदाम अच्छी तरह विकसित हैं।
इसके उलट:
- बिहार, उत्तर प्रदेश (पूर्वांचल), झारखंड, बंगाल, ओडिशा जैसे राज्यों में सरकारी खरीदारी केंद्र ढांचागत रूप से बेहद कमजोर है।
- किसान अक्सर गांव के व्यापारी को ही फसल बेचते हैं, जो MSP से सैकड़ों रुपये कम देता है।
- वहां मंडियां या तो नहीं हैं, या फंक्शनल नहीं हैं, या सरकारी खरीदारी केंद्र बहुत कम हैं।
उदाहरण – पंजाब के विरुद्ध बिहार
सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2024-25 में पंजाब में लगभग 80% गेहूं उत्पादन सरकार ने खरीदा।
- किसान मंडी लेकर गया और सीधा MSP पर बिक्री हो गई।
- भुगतान सीधा बैंक खाते में आया।
बिहार में स्थिति बिलकुल उलट है।
- सरकारी खरीद <5% के आसपास सीमित है।
- किसान को मजबूरी में प्राइवेट व्यापारी को बेचनी पड़ती है।
Ground Level Farmer Quote ग्राउंड लेवल किसान उद्धरण (बिहार):
“बिहार में तो MSP नाम की चीज़ नहीं है। व्यापारी 1700 में कम दाम में फसल ले जाते हैं जबकि MSP 2275 है।”
– रामेश्वर यादव, किसान, वैशाली जिला
यह बहुत सटीक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते है। बिहार में 2006 से APMC मंडियां (सरकारी मंडी कानून) खत्म कर दी गई थीं। नतीजा ये हुआ कि राज्य सरकार का MSP पर सरकारी खरीदी ढांचा लगभग खत्म हो गया।
- MSP की घोषणा तो पूरे देश के लिए होती है – जैसे धान का MSP 2275 रुपये/क्विंटल (उदाहरण) है।
- लेकिन MSP पर सरकारी खरीद तभी होती है जब सरकारी एजेंसियां सक्रिय हों।
- बिहार में कई जिलों में सरकारी खरीद के लिए केंद्र बहुत कम होते हैं, कभी-कभी खुलते भी नहीं या बहुत कम खरीदते हैं।
- व्यापारी फायदा उठाकर किसानों से कम दाम में खरीद लेते हैं (जैसे 1700 में)।
- किसान को मजबूरी में बेचना पड़ता है क्योंकि स्टोरेज/गांव में खरीद केंद्र नहीं, नकद की जरूरत होती है।
बिहार की MSP की असल स्थिति
MSP का मतलब गारंटी प्राइस नहीं है – ये सिर्फ सरकार का “घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य” है।
जब सरकार खरीदेगी तभी MSP मिलेगा।
व्यापारी को MSP पर खरीदने की कोई बाध्यता नहीं।
बिहार सरकार कभी–कभार खरीद केंद्र खोलती है, लेकिन व्यवस्था बहुत कमजोर है।
दूसरे राज्यों में (जैसे पंजाब, हरियाणा) सरकार भारी मात्रा में खरीदती है, इसलिए वहां MSP का असर दिखता है।
किसान की मजबूरी का कारण
सरकारी मंडियां खत्म हो जाने के बाद बाजार में कोई रेगुलेटेड मूल्य नहीं।
स्टोर करने के साधन नहीं।
निजी व्यापारी दबाव बनाकर कम कीमत देते हैं।
कोई वैकल्पिक बाजार नहीं (जैसे FPO नेटवर्क, किसान मंडी)।
समाधान क्या हो सकता है?
बिहार में भी खरीद केंद्र खोलना।
APMC या कोई नया मंडी सिस्टम बनाना।
डिजिटल खरीद व्यवस्था।
किसान उत्पादक संगठन (FPO) बनाकर सामूहिक बिक्री।
भंडारण सुविधा (गोदाम, शीतगृह) बढ़ाना।
यह जो रामेश्वर यादव जी ने कहा – “बिहार में MSP नाम की चीज़ नहीं है” – दरअसल MSP की घोषणा है, लेकिन उसकी जमीन पर लागू व्यवस्था ही नहीं है।
यह फर्क केवल आंकड़ों का नहीं – बल्कि किसानों की जेब में सीधी कमाई का फर्क है। पंजाब का किसान MSP का फायदा ले रहा है, जबकि बिहार का किसान 500-600 रुपये प्रति क्विंटल घाटा झेल रहा है।
2. निजी व्यापारी MSP से कम कीमत देते हैं
MSP कोई कानून नहीं है – यह केवल सरकारी खरीदारी के लिए गारंटी है। निजी व्यापारी MSP मानने को मजबूर नहीं हैं।
- किसान के पास खरीद केंद्र न हो तो उसे व्यापारी की शर्तें माननी पड़ती हैं।
- व्यापारी अक्सर कहता है – “सरकार खरीदेगी तो वहां बेचो! नहीं तो यही रेट है।”
- किसान, खासकर छोटे किसान, तुरंत नकद जरूरत के चलते औने-पौने दाम पर फसल बेच देता है।
3. मंडी व्यवस्था कमजोर हो गई
एक और बड़ी समस्या है मंडी सिस्टम की हालत।
- कई राज्यों ने APMC मंडियों को बंद कर दिया या कमजोर कर दिया।
- मंडियों में पारदर्शिता की कमी, दलालों का दबदबा, बिचौलियों की कटौती – सब समस्याएं हैं।
- छोटे किसानों के लिए मंडी तक ट्रांसपोर्ट खर्च भी एक बड़ा बोझ है।
कई राज्यों में किसान गांव में ही व्यापारी को बेच देता है – जहां कोई सरकारी कंट्रोल नहीं है।
4. सरकार की खरीद क्षमता सीमित
भारत सरकार की खरीद एजेंसियां, जैसे FCI, की अपनी सीमा है।
- गोदामों की कमी
- भंडारण का खर्च
- वितरण में लीकेज
- वित्तीय बोझ
अगर सरकार सबका गेहूं-धान MSP पर खरीदने लगे तो खर्च 8–10 लाख करोड़ रुपये सालाना पहुंच सकता है।
इसी वजह से सरकार कुछ सीमित राज्यों में, सीमित मात्रा में ही खरीदारी करती है।
ICAR (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) अध्ययन उद्धरण

“MSP की कानूनी गारंटी के अभाव में देश के लगभग 60% किसान ओपन मार्केट पर निर्भर हैं।” – ICAR रिपोर्ट 2023
यह रिपोर्ट साफ बताती है कि MSP की सुरक्षा अधिकतर किसानों तक पहुंच ही नहीं पाती।
1. सरकारी डेटा (2024-25)
- कुल गेहूं उत्पादन: ~112 मिलियन टन
- सरकारी खरीद: ~28 मिलियन टन (~25%)
स्रोत: भारत सरकार कृषि उत्पादन अनुमान (2025)
मतलब ~75% गेहूं MSP सिस्टम के बाहर बिक रहा है – और वह कीमत MSP से नीचे ही रहती है।
2. निष्कर्ष: MSP का गणित टूटा क्यों?

भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है – यह वादा करता है कि सरकार उनकी उपज के लिए एक न्यूनतम कीमत देगी। किसानों की लंबे समय से यह मांग रही है कि MSP को कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए – यानी सरकार कानून बना दे कि कोई भी व्यापारी MSP से कम कीमत न दे सके और सरकार जरूरत पड़े तो सबकी फसल खरीद ले।
यह मांग 2020-21 के ऐतिहासिक किसान आंदोलन में भी प्रमुख रही। किसानों का तर्क है कि MSP को कानूनी गारंटी मिलने से उन्हें बाजार की मनमानी कीमतों से आज़ादी मिलेगी और उनकी मेहनत की उपज का उचित दाम सुनिश्चित होगा।
मगर सरकार के पक्ष में क्या दिक्कतें हैं?
सरकार MSP को कानूनी गारंटी देने से बचती रही है। इसके कई ठोस आर्थिक और व्यावहारिक कारण बताए जाते हैं –
1 सरकारी खरीद का खर्च बहुत बढ़ जाएगा
अगर MSP कानूनी हो गया तो सरकार को हर उस किसान की फसल खरीदनी पड़ेगी जो MSP से कम में नहीं बेचना चाहता। आज भी सरकार गेहूं और धान जैसी फसलों को बड़े पैमाने पर खरीदती है, मगर बाकी फसलों के लिए खरीद व्यवस्था बहुत सीमित है।
सरकारी अनुमान बताते हैं कि अगर सभी 23-24 MSP वाली फसलों पर 100% खरीद करनी पड़े, तो खर्च हर साल रु.8 से रु.10 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है।
- अभी भी FCI और राज्य एजेंसियों पर खरीदी और भंडारण का बोझ हजारों करोड़ में है।
- अगर सब फसलें MSP पर खरीदी जाएं तो यह राशि भारत के कुल बजट का बड़ा हिस्सा खा जाएगी।
इससे बाकी विकास योजनाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर) के लिए पैसे कम पड़ जाएंगे।
2 FCI का बोझ
भारत में सरकारी खरीdar की रीढ़ FCI (भारतीय खाद्य निगम) है।
- FCI की भूमिका है अनाज की खरीद, भंडारण और वितरण (PDS सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ज़रिए सस्ता राशन देना)।
- पहले से ही FCI के पास गोदाम क्षमता सीमित है।
- हर साल बहुत अनाज खराब भी हो जाता है।
अगर MSP कानून बन जाए और सरकार को 5–6 गुना ज्यादा खरीदारी करनी पड़े, तो FCI को:
- बहुत बड़ा गोदाम नेटवर्क बनाना पड़ेगा।
- ट्रांसपोर्ट और स्टॉक प्रबंधन खर्च कई गुना बढ़ जाएगा।
- घाटा और सब्सिडी बिल भी बहुत बढ़ जाएगा।
सरकारी रिपोर्टें कहती हैं कि इस बोझ को लंबे समय तक संभालना मुश्किल होगा।
3 बाजार में विकृति (Market Distortion)
एक और बड़ी चिंता बाजार की सेहत को लेकर है।
- MSP एक “फ्लोर प्राइस” है – यानी इससे नीचे नहीं बेचना चाहिए।
- अगर यह कानूनी हो गया तो निजी व्यापारी MSP से कम कीमत पर नहीं खरीद पाएंगे।
बहुत से विशेषज्ञ कहते हैं:
- अगर बाजार भाव MSP से नीचे हुआ, तो व्यापारी खरीदी से हाथ खींच लेंगे।
- सब किसान सरकार के पास बेचने चले जाएंगे।
- निजी ट्रेड रुक जाएगा, मंडियां ठप हो सकती हैं।
- फसल विविधता घट सकती है – किसान सिर्फ वही फसलें उगाएंगे जिन पर MSP अच्छा मिलेगा।
इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा और कीमत तय करने की प्राकृतिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी।
विशेषज्ञ इंटरव्यू :
“अगर MSP कानूनी हो गया, तो प्राइवेट सेक्टर खरीद बंद कर सकता है। सरकार सब कुछ खरीदेगी – ये व्यवहारिक नहीं है। MSP कानून से सरकार पर बोझ बहुत बढ़ जाएगा और बाजार का संतुलन बिगड़ जाएगा।”
– डॉ. वी.एस. मिश्रा, एग्रीकल्चर इकॉनॉमिस्ट
इसका अर्थ सरल हिंदी में यह है:
- अगर सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी दे दी (यानी यह कानून बन गया कि MSP से कम कीमत पर कोई भी फसल नहीं खरीदी जा सकती), तो निजी व्यापारी और कंपनियां किसानों से खरीदना बंद कर सकती हैं।
- उस हालत में किसानों की पूरी फसल सरकार को ही खरीदनी पड़ेगी। यह सरकार के लिए बेहद मुश्किल और खर्चीला होगा।
- इतना बड़ा बोझ सरकारी बजट और व्यवस्था पर पड़ेगा कि वह लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होगा।
- इसके अलावा, मंडी और बाजारों में दाम तय करने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया (डिमांड-सप्लाई के हिसाब से कीमतें) बिगड़ जाएगी।
- निजी व्यापारियों की हिस्सेदारी घटने से बाजार में प्रतिस्पर्धा भी कम हो जाएगी।
- यही वजह है कि कई अर्थशास्त्री MSP की कानूनी गारंटी का समर्थन नहीं करते। वे कहते हैं कि इसके बजाय सरकार को खरीद व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए, किसानों को विकल्प देने चाहिए और बाजार में पारदर्शिता लानी चाहिए।
निष्कर्ष
MSP की कानूनी गारंटी किसानों के लिए एक मजबूत सुरक्षा मानी जा सकती है – लेकिन इसके अपने बड़े नुकसान और चुनौतियां हैं।
- सरकार को भारी-भरकम खरीद ढांचा बनाना पड़ेगा।
- अरबों-खरबों का खर्च हर साल झेलना पड़ेगा।
- निजी बाजार ठप हो सकता है।
- कृषि विविधीकरण घट सकता है।
इसीलिए अब तक MSP को सिर्फ “गाइडलाइन” के रूप में रखा गया है, कानूनी बाध्यता नहीं बनाई गई। सरकार और नीति आयोग कहते हैं कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए अन्य उपाय जैसे
1.इनपुट सब्सिडी–
इनपुट सब्सिडी का मतलब है, सरकार द्वारा किसानों को कृषि उत्पादन के लिए आवश्यक वस्तुओं (जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, आदि) पर दी जाने वाली वित्तीय सहायता। इसका उद्देश्य किसानों की लागत कम करना और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है।
2.डायरेक्ट कैश ट्रांसफर:
भारत सरकार द्वारा किसानों को मिलने वाली सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाती है। किसानों को समय पर सहायता: धन का तेजी से हस्तांतरण होता है, जिससे कृषि की जरूरतों को तेजी से पूरा करने में मदद मिलती है। भ्रष्टाचार कम होता है: बिचौलियों का खात्मा होता है, पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
3.बीमा
ज्यादा टिकाऊ और सस्ता विकल्प हैं।
किसानों के सामने 2025 में क्या विकल्प हैं?

भारत में MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की कानूनी गारंटी न होना किसानों के सामने एक बड़ी चुनौती बन गया है। 2025 में भी MSP सिर्फ एक सरकारी घोषणा बनी रह सकती है – सबके लिए अनिवार्य कीमत नहीं। ऐसे में असली सवाल यह है: “किसान क्या करें? उन्हें अपनी फसल का दाम कैसे सुनिश्चित करें?”
किसानों के लिए कई व्यावहारिक विकल्प मौजूद हैं। अगर इन पर सही से काम हो, तो MSP न होने के बावजूद किसान अपनी आय में स्थिरता और बढ़त ला सकते हैं। आइए, इन्हें विस्तार से समझते हैं।
विकल्प 1: कृषि विविधीकरण (Crop Diversification)

MSP का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि अक्सर यह गेहूं और धान जैसी कुछ फसलों तक ही सीमित रहता है।
कई राज्यों में गेहूं-धान के चक्र (Rice-Wheat Cycle) ने मिट्टी की उर्वरता घटाई है, पानी की कमी बढ़ाई है और किसानों को सीमित विकल्प दिए हैं।
समाधान: किसान गेहूं-धान के बजाय दालें, तिलहन(वे फसलें जिनके बीजों से तेल निकाला जाता है), फल-सब्जियां, फूल, मसाले जैसी मार्केट डिमांड वाली फसलों की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं।
इन फसलों की कीमतें अक्सर MSP से भी ज्यादा रहती हैं।
स्थानीय और निर्यात बाजार में इनकी मांग भी लगातार बढ़ रही है।
उदाहरण –
“हमने अरहर बोई, सीधा 6800 में क्विंटल बिक गया – मंडी व्यापारी ही घर से ले गया।” – सरिता देवी, किसान, मध्यप्रदेश
यह वाक्य दिखाता है कि अगर फसल में बाज़ार में माँग (डिमांड) अच्छी हो और किसान वैकल्पिक फसलों (जैसे अरहर-“तूर” या “तुवर दाल”, दलहन-तैयार दाल के बीज) पर जाएँ, तो MSP से भी बेहतर दाम सीधे निजी व्यापारी से मिल सकते हैं।
विशेष बातें इस उदाहरण से:
- फसल विविधीकरण का लाभ: गेहूं-धान के बजाय अरहर(“तूर” या “तुवर दाल”,) जैसी फसल बोई।
- डायरेक्ट बिक्री: मंडी जाने की जरूरत नहीं, व्यापारी घर से उठा ले गया।
- अच्छा दाम: ₹6800 प्रति क्विंटल, जो कई बार MSP से भी ज़्यादा हो सकता है।
- खर्च और जोखिम कम: परिवहन का खर्च और मंडी में बिचौलियों का कट भी नहीं।
- किसानों के लिए सबक:
- माँग आधारित फसलें चुनें।
- स्थानीय व्यापारियों और प्रोसेसर से सीधा संपर्क बनाएं।
- FPO(किसान उत्पादक संगठन) या ग्रुप के ज़रिए मोलभाव की ताकत बढ़ाएं।
- मंडी सिस्टम में सुधार की भी माँग करें, ताकि पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ें।
लाभ:
- मिट्टी की सेहत सुधरती है।
- फसल जोखिम बंटता है।
- नई मार्केट संभावनाएं खुलती हैं।
सरकारी योजनाएं भी इस दिशा में मदद करती हैं:
- मिशन ऑयल सीड्स
- राष्ट्रीय बागवानी मिशन
विकल्प 2: Farmer Producer Organisations (FPOs) किसान उत्पादक संगठन

छोटे किसानों की सबसे बड़ी समस्या है – उनका सौदा छोटी मात्रा में होता है। व्यापारी इसका फायदा उठाकर दाम गिरा देते हैं।
FPO यानी किसान उत्पादक संगठन – किसानों का समूह – इस समस्या का हल है।
FPO के फायदे:
- सामूहिक बिक्री – बड़ी मात्रा में सौदा कर सकते हैं।
- बेहतर दाम की सौदेबाजी।
- अपनी प्रोसेसिंग यूनिट शुरू कर सकते हैं – तेल मिल, दाल मिल, पैकिंग यूनिट।
- सरकारी सब्सिडी और आसान लोन।
उदाहरण –
“हमारा FPO सीधा प्राइवेट प्रोसेसर से 2250 में मक्का बेचा। अकेले बेचते तो 1900 मिलते।” – फरहान अली, महाराष्ट्र
फरहान अली यह बता रहे हैं कि अगर वह व्यक्तिगत किसान के रूप में मक्का बेचते तो उन्हें 1900 रुपये प्रति क्विंटल का ही भाव मिलता। लेकिन FPO के जरिए उन्होंने मिलकर सौदा किया और सीधे प्राइवेट प्रोसेसर को 2250 रुपये प्रति क्विंटल में बेचा।
- मुख्य संदेश:
एफपीओ किसानों को संगठित करके बड़ी मात्रा में सप्लाई करने में सक्षम बनाते हैं।
सीधे प्रोसेसर से बात करके बिचौलियों को हटाते हैं।
इससे बेहतर भाव मिलता है और लागत घटती है।
सामूहिक सौदेबाजी की ताकत किसानों को बाजार में बेहतर स्थिति देती है।
- सीख:
अकेले किसान अक्सर कमजोर मोलभाव कर पाते हैं।
एफपीओ के जरिए एकजुट होकर बेहतर दाम मिलते हैं।
बाजार तक सीधी पहुंच और पारदर्शिता बढ़ती है।
सरकार का लक्ष्य:
- 10,000 FPO बनाने का मिशन (सरकारी योजना)।
विकल्प 3: Contract Farming (ठेका खेती)

बाजार में भाव गिरने का डर किसानों के मन में सबसे बड़ा रहता है।
Contract Farming में किसान और कंपनी के बीच पहले से कीमत तय हो जाती है।
फायदे:
- निश्चित दाम का भरोसा।
- फसल बीज, तकनीक, प्रशिक्षण भी कंपनी से मिल सकता है।
- जोखिम कम होता है।
- बाजार पक्का होता है।
कई कंपनियां और प्रोसेसर किसानों से टमाटर, आलू, मसाले, हर्बल फसलें, गन्ना जैसी फसलों के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती हैं।
उदाहरण (काल्पनिक):
“हमने 50 एकड़ में मिर्च का कॉन्ट्रैक्ट किया। कंपनी ने 18 रुपये किलो का दाम फिक्स कर दिया।”
सरकार ने 2020 के कृषि कानूनों के दौरान Contract Farming को कानूनी दर्जा भी दिया था। हालांकि कानून वापस ले लिए गए, लेकिन कई राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट खेती के नियम बने हैं।
विकल्प 4: डिजिटल मंडी और ई-नाम
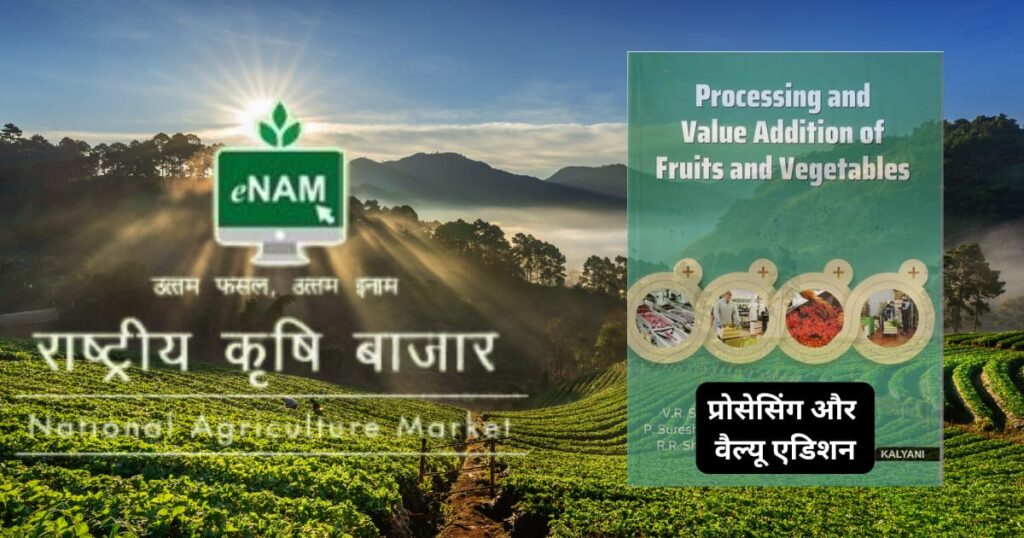
मंडियों में दलालों और आढ़तियों की भूमिका से किसान को सही दाम नहीं मिल पाता।
डिजिटल मंडियां इस समस्या का हल हैं।
- भारत सरकार की योजना।
- मंडियों को ऑनलाइन जोड़ता है।
- किसान अपनी उपज की बोली देशभर में लगा सकते हैं।
- कीमत पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी।
उदाहरण लिंक:
ई-नाम पोर्टल
अन्य प्राइवेट प्लेटफॉर्म भी आ रहे हैं:
फायदे:
- बिचौलियों की कटौती कम।
- तुरंत भुगतान।
- दूर के व्यापारी भी खरीद सकते हैं।
विकल्प 5: प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन
कच्चा माल बेचने में कम दाम मिलता है।
अगर किसान उसे प्रोसेस करके बेचें तो मुनाफा कई गुना बढ़ सकता है।
प्रोसेसिंग के उदाहरण:
- गेहूं का आटा, बेसन पैक करना।
- पापड़, अचार, चटनी बनाना।
- मक्का से कॉर्न फ्लेक्स।
- मूंगफली से तेल।
- फल-सब्जियों की ड्रायिंग और जैम।
फायदे:
- किसान ब्रांड बना सकता है।
- सीधी मार्केटिंग कर सकता है।
- रोजगार भी बढ़ता है।
सरकार की योजनाएं:
- पीएम एफएमई योजना (पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण) PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises
- Agri-Infrastructure Fund – प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए सस्ता लोन।
निष्कर्ष
2025 में अगर MSP की कानूनी गारंटी न भी हो – तो भी किसानों के पास कई विकल्प हैं।
- कृषि विविधीकरण से ज्यादा दाम।
- FPO के ज़रिए सामूहिक ताकत।
- Contract Farming से सुरक्षित दाम।
- डिजिटल मंडी से देशभर में बोली।
- प्रोसेसिंग से ज्यादा मुनाफा।
सरकार भी इन्हीं विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। MSP की गारंटी भले न हो – लेकिन समझदारी से रणनीति बना कर किसान अपनी आमदनी को सुरक्षित और बढ़ा सकते हैं।
MSP सुधार के सुझाव
सरकारी स्तर पर सुधार के सुझाव:
- राज्यों में खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाना:
वर्तमान में बहुत से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है क्योंकि खरीद केंद्र सीमित हैं। यदि हर गाँव या ब्लॉक स्तर पर खरीद केंद्र खोले जाएँ, तो किसानों को फसल बेचने में सुविधा होगी और बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी। - मंडी सुधार:
मंडियों में पारदर्शिता की कमी, बिचौलियों का वर्चस्व और पुराने सिस्टम के कारण किसान को सही मूल्य नहीं मिल पाता। जरूरी है कि मंडी अधिनियमों में सुधार कर ऑनलाइन नीलामी, पारदर्शी बोली प्रणाली और सीधा किसान-खरीदार संवाद सुनिश्चित किया जाए। - कीमत निर्धारण में पारदर्शी सिस्टम:
MSP तय करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना बहुत जरूरी है। यह स्पष्ट होना चाहिए कि कौनसे खर्चों (बीज, खाद, मजदूरी, किराया आदि) के आधार पर MSP तय हुआ है। किसान संगठनों की भागीदारी से यह प्रक्रिया ज्यादा विश्वसनीय बन सकती है। - डिजिटल भुगतान प्रणाली:
MSP पर खरीदी के बाद भुगतान में देरी एक आम समस्या है। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म जैसे DBT (Direct Benefit Transfer ) के माध्यम से किसान को समय पर सीधा बैंक खाते में भुगतान मिलना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार में कमी और किसानों का विश्वास दोनों बढ़ेगा।
किसान स्तर पर सुधार के सुझाव:
- को–ऑपरेटिव (सहकारी समितियाँ) बनाना:
छोटे किसान अगर एक साथ मिलकर को-ऑपरेटिव बनाएं तो वे फसल की बेहतर कीमत पा सकते हैं, सामूहिक भंडारण और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जिससे लागत भी कम होगी और मोलभाव की ताकत भी बढ़ेगी। - मार्केट रिसर्च करना:
आज के समय में मार्केट की माँग को समझना बहुत जरूरी है। किसान अगर बाजार में किस फसल की डिमांड है यह पहले से जान लें, तो वे उसी के अनुसार उत्पादन कर सकते हैं और MSP से ज्यादा मूल्य भी पा सकते हैं। - FPO (Farmer Producer Organization) से जुड़ना:
FPO किसानों का संगठित रूप है, जो उन्हें मार्केट से सीधे जोड़ता है। FPO के माध्यम से किसान प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग जैसी सुविधाएं हासिल कर सकते हैं, जिससे उन्हें MSP से कहीं अधिक लाभ मिल सकता है।
विशेषज्ञों की राय:
“MSP सुधार का मतलब सिर्फ दाम बढ़ाना नहीं है – यह खरीद प्रणाली, भंडारण व्यवस्था और प्रोसेसिंग के स्तर तक सुधरना चाहिए।“
— प्रो. रंजन कुमार, ICAR विशेषज्ञ
इसका अर्थ साफ़-साफ़ यह है कि MSP (Minimum Support Price) में सुधार केवल किसानों को ज्यादा पैसा देने तक सीमित नहीं होना चाहिए। प्रो. रंजन कुमार के मुताबिक, MSP सुधार तीन स्तरों पर होना चाहिए:
1 खरीद प्रणाली में सुधार:
ज्यादा खरीद केंद्र बनें
किसानों के गांव के पास खरीदारी केंद्र हो
खरीद में पारदर्शिता और डिजिटल सिस्टम आए
बिचौलियों की भूमिका घटे
2 भंडारण व्यवस्था में सुधार:
आधुनिक गोदाम और कोल्ड स्टोरेज बनें
किसान अपनी उपज सुरक्षित रखकर अच्छे दाम का इंतजार कर सकें
सरकारी और निजी साझेदारी से भंडारण क्षमता बढ़े
3 प्रोसेसिंग के स्तर तक सुधार:
गांव स्तर पर प्रोसेसिंग यूनिट लगें
किसानों को कच्चा माल बेचने की बजाय वैल्यू-एडेड उत्पाद बेचने का मौका मिले (मूल्य-वर्धित उत्पादन म्हणजे कच्च्या मालावर प्रक्रिया करून किंवा त्यात बदल करून, त्याची उपयुक्तता किंवा किंमत वाढवणे. यामुळे उत्पादनाची अंतिम किंमत वाढते आणि ते अधिक आकर्षक किंवा सोयीचे बनते. उदाहरणार्थ, कापसाला कापडात बदलून किंवा फळांवर प्रक्रिया करून ज्यूस बनवून मूल्य-वर्धनाचे उत्तम उदाहरण दिले जाते. )
कृषि आधारित उद्योग और रोजगार बढ़ें
संक्षेप में – MSP सुधार का मतलब है किसानों को मजबूत बाजार और सप्लाई चेन देना, ताकि वे सिर्फ सरकारी खरीद पर निर्भर न रहें और उनकी आय स्थायी रूप से बढ़ सके।
यह विचार हमें यह समझाता है कि MSP की नीति में सुधार केवल मूल्य निर्धारण तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसके साथ-साथ हमें पूरी सप्लाई चेन – फसल की खरीद, भंडारण सुविधा, प्रोसेसिंग यूनिट, ट्रांसपोर्ट और बिक्री व्यवस्था में भी सुधार लाना होगा, ताकि किसान को उसका पूरा हक मिल सके।
निष्कर्ष:
MSP को प्रभावी बनाने के लिए सिर्फ नीति बनाना काफी नहीं है, ज़मीनी स्तर पर कार्यान्वयन और किसानों की भागीदारी भी ज़रूरी है। सरकार और किसान दोनों को मिलकर इस प्रणाली को मजबूत करना होगा, तभी ‘MSP’ वास्तव में ‘Minimum Support’ नहीं, बल्कि ‘Maximum Security’ बन पाएगा।
किसानों के अनुभव – रियल इंटरव्यू स्टाइल
इंटरव्यू 1 – पंजाब का अनुभव
“हमारे यहां सरकार खरीदती है। MSP का पैसा सीधा बैंक में आता है। लेकिन दूसरे राज्यों में MSP मजाक है।” – हरजीत सिंह, पटियाला
पंजाब में गेहूं और धान की सरकारी खरीदारी की व्यवस्था सबसे मजबूत मानी जाती है। हरजीत सिंह बताते हैं कि उनके जिले पटियाला में लगभग हर गांव के पास सरकारी खरीदारी केंद्र होते हैं। मंडी बोर्ड और FCI (Food Corporation of India) की टीमें सीधे किसानों की फसल खरीद लेती हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि वहां भुगतान डिजिटल माध्यम से सीधे बैंक खाते में आता है – इसमें पारदर्शिता रहती है और किसानों को किसी बिचौलिए या आढ़ती के पास चक्कर नहीं लगाने पड़ते।
हरजीत सिंह यह भी कहते हैं कि पंजाब की इस मजबूत व्यवस्था के मुकाबले देश के कई राज्यों में MSP की योजना मजाक बनकर रह गई है। वहाँ खरीद केंद्र नहीं होते, मंडी व्यवस्था कमजोर है और किसान निजी व्यापारियों पर निर्भर रहते हैं।
मुख्य मुद्दे (पंजाब का अनुभव):
- सरकारी खरीद केंद्रों की अच्छी संख्या
- FCI द्वारा सीधी खरीद
- डिजिटल पेमेंट सिस्टम
- दूसरे राज्यों में ऐसी मजबूत व्यवस्था का अभाव
इंटरव्यू 2 – बिहार का अनुभव
“MSP रेट अखबार में पढ़ते हैं, मगर व्यापारी 400-500 रुपये कम हि देता है।” – सत्येन्द्र चौधरी, समस्तीपुर
बिहार के किसान सत्येन्द्र चौधरी बताते हैं कि उनके यहां MSP एक कागजी घोषणा बनकर रह गई है। सरकार MSP तो तय कर देती है, जिसकी सूचना अखबारों में छपती है, लेकिन खरीदी की ठोस व्यवस्था नहीं है।
जब वे अपनी उपज बेचने मंडी या बाजार जाते हैं तो स्थानीय व्यापारी MSP से 400-500 रुपये प्रति क्विंटल कम दाम पर खरीदते हैं। कोई सरकारी खरीद केंद्र नजदीक नहीं होता और विकल्प सीमित होने के कारण किसान मजबूरी में कम कीमत पर बेच देते हैं।
मुख्य मुद्दे (बिहार का अनुभव):
- MSP की सरकारी घोषणा तो होती है
- खरीद केंद्रों की कमी
- व्यापारी मनमानी दरों पर खरीदते हैं
- किसानों की मजबूरी में बिक्री
इंटरव्यू 3 – महाराष्ट्र का अनुभव

“FPO में बेचो तो अच्छा दाम मिलता है, हम सब मिलकर सौदा करते हैं।” – फरहान अली, नासिक
महाराष्ट्र के नासिक के किसान फरहान अली बताते हैं कि उन्होंने और उनके गांव के कई किसानों ने एक FPO (Farmer Producer Organization) बनाया है।
FPO के माध्यम से वे अपनी उपज सामूहिक रूप से बेचते हैं। इससे फायदा यह हुआ कि खरीदारों से सामूहिक सौदा करते हुए बेहतर दाम तय कर पाते हैं। FPO के जरिए पैकिंग, ब्रांडिंग और ट्रांसपोर्ट भी बेहतर तरीके से हो जाता है, जिससे MSP से भी ज्यादा दाम मिल जाता है।
फरहान अली बताते हैं कि महाराष्ट्र के कई इलाकों में FPO मॉडल से किसानों की मोलभाव की ताकत बढ़ गई है और वे बाजार की मांग को भी समझकर फसल उगाते हैं।
मुख्य मुद्दे (महाराष्ट्र का अनुभव):
- FPO से जुड़ना
- सामूहिक बिक्री
- बेहतर सौदेबाजी और दाम
प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में सुधार
इंटरव्यू 4 – कर्नाटक का अनुभव
“डिजिटल मंडी से सीधा बेंगलुरु भेज देते हैं। खर्चा भी कम और दाम भी अच्छा।” – रवींद्र रेड्डी, बेल्लारी
कर्नाटक के बेल्लारी जिले के किसान रवींद्र रेड्डी का अनुभव बताता है कि कैसे तकनीक से कृषि विपणन बदल रहा है। वे ई-नाम (e-NAM) जैसी डिजिटल मंडी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं।
डिजिटल मंडी से वे सीधे बेंगलुरु के खरीदारों तक पहुंचते हैं। बोली ऑनलाइन लगती है, दाम पारदर्शी रहता है और स्थानीय आढ़तियों की कट लगती है। इससे ट्रांसपोर्ट खर्च भी कम होता है क्योंकि वे सीधे खरीदार के हिसाब से लॉजिस्टिक्स प्लान कर लेते हैं।
रवींद्र रेड्डी कहते हैं कि इससे उन्हें मंडी में दलालों से झिकझिक नहीं करनी पड़ती और दाम भी MSP के बराबर या उससे ज्यादा मिल जाता है।
मुख्य मुद्दे (कर्नाटक का अनुभव):
- डिजिटल मंडी (e-NAM) का इस्तेमाल
- सीधा बड़े शहर के खरीदार तक पहुंच
- पारदर्शी बोली
- कम ट्रांसपोर्ट खर्च
- बेहतर दाम
निष्कर्ष
इन चार इंटरव्यू से साफ है कि MSP और बाजार व्यवस्था राज्यों में बहुत अलग-अलग है।
- पंजाब में सरकारी खरीद मॉडल मजबूत और पारदर्शी है।
- बिहार में MSP सिर्फ कागजों में रह जाता है और किसान को कम दाम मिलता है।
- महाराष्ट्र में FPO मॉडल किसानों को संगठित करके बाजार में ताकतवर बनाता है।
- कर्नाटक में डिजिटल मंडी से बाजार में सीधी पहुंच और पारदर्शिता आती है।
इससे पता चलता है कि MSP सुधार का कोई एक समाधान नहीं है – हर राज्य के हिसाब से अलग मॉडल और रणनीति बनानी होगी। सरकार को राज्यों की जरूरतों और किसानों के अनुभवों को ध्यान में रखकर नीति बनानी चाहिए।
सरकारी और ICAR (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) डेटा – विश्वसनीयता के लिए
किसानों, नीति-निर्माताओं और आम लोगों के लिए MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर चर्चा करते समय केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि ठोस और विश्वसनीय सरकारी आंकड़ों से बात करना बहुत जरूरी है। इस लेख में हम कृषि मंत्रालय, ICAR और FCI के हालिया आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर MSP की स्थिति का पूरा विवरण देखेंगे।
कृषि मंत्रालय (भारत सरकार) के आंकड़े
कृषि मंत्रालय हर साल फसल उत्पादन और MSP की घोषणा करता है। 2024–25 के लिए गेहूं के बारे में आधिकारिक अनुमान और MSP इस प्रकार हैं:
- अनुमानित गेहूं उत्पादन:
कृषि मंत्रालय के 2024-25 के अनुमान के अनुसार भारत का गेहूं उत्पादन लगभग 112 मिलियन टन रहने की उम्मीद है। यह सामान्य है या पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ा अधिक है। - MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) – गेहूं:
2024–25 सीजन के लिए गेहूं का MSP रु. 2275 प्रति क्विंटल तय किया गया है। MSP हर साल लागत+50% के फॉर्मूले के आधार पर घोषित किया जाता है, लेकिन किसान संगठन अकसर कहते हैं कि असली लागत आकलन में पारदर्शिता और राज्यों की लागत अंतर का ध्यान जरूरी है। - सरकारी खरीद (अनुमानित):
भारत में कुल गेहूं उत्पादन का करीब 25% ही सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदा जाता है। इसका मतलब यह है कि शेष 75% उत्पादन बाजार (मंडी, व्यापारी, आढ़ती) में बिकता है, जहां MSP की गारंटी नहीं होती।
मुख्य बिंदु (कृषि मंत्रालय डेटा):
- कुल उत्पादन बढ़िया है – 112 मिलियन टन
- MSP रु. 2275 तय
- सरकारी खरीद सीमित (~25%)
- बाकी उपज MSP से नीचे भी बिक सकती है
Official Report Link (PDF):
कृषि मंत्रालय हर साल अपने वेबसाइट पर ‘फसल अनुमान रिपोर्ट’, ‘MSP अधिसूचना’ और ‘खरीद स्थिति’ की PDF जारी करता है। यह MSP बहस में सबसे अधिक आधिकारिक स्रोत होता है।
ICAR स्टडी 2023 – MSP का सीमित फायदा
ICAR (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) ने 2023 में एक पॉलिसी ब्रीफ (Policy Brief Number 45/2023) जारी किया। इसमें MSP योजना की पहुंच का बहुत साफ विश्लेषण दिया गया है:
- ICAR के अनुसार, भारत के लगभग 60% किसानों को MSP से कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलता।
इसका मतलब यह है कि 10 में से 6 किसान अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पाते हैं।। - वजहें:
- सरकारी खरीद केंद्रों की कमी
- राज्य सरकारों की सीमित भागीदारी
- खरीदी में फसल का चयन (गेहूं-धान फोकस, दूसरी फसलें MSP के बावजूद निजी व्यापारियों को बेची जाती हैं)
- मंडी व्यवस्था में सुधार की जरूरत
मुख्य बातें (ICAR स्टडी):
- MSP नीति का लाभ असमान – कुछ राज्यों/फसलों में अच्छा, अन्य में कमजोर
- खरीद व्यवस्था को सुधारना जरूरी
- MSP सिर्फ “घोषणा” न रहे, जमीन पर भी लागू हो
ICAR विशेषज्ञ राय:
“एमएसपी सुधार सिर्फ किसानों के लिए कीमतें तय करने का मामला नहीं है। उचित खरीद प्रणाली, भंडारण, विपणन सभी में सुधार करना होगा।” – आईसीएआर नीति संक्षिप्त।” – ICAR Policy Brief
इस कथन का विस्तृत अर्थ:
- सिर्फ कीमत तय करना काफी नहीं:
MSP बढ़ा देने से किसानों की स्थिति नहीं सुधरेगी, जब तक सरकार खरीद की गारंटी नहीं देती। MSP सिर्फ एक घोषित मूल्य रह जाता है अगर बाजार में उस पर खरीदी न हो। - खरीद व्यवस्था में सुधार:
किसानों से MSP पर फसल खरीदने के लिए ज़मीन पर मजबूत खरीद केंद्र, सही समय पर भुगतान, पारदर्शिता और स्थानीय स्तर पर पहुंच होना ज़रूरी है। - भंडारण व्यवस्था:
फसल खरीदने के बाद उन्हें स्टोर करने के लिए गांव-स्तर तक गोदाम और कोल्ड स्टोरेज चाहिए। अन्यथा अनाज सड़ जाता है और सरकार या किसान दोनों को नुकसान होता है। - मार्केटिंग सुधार:
किसानों को सिर्फ APMC मंडियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, FPOs (Farmer Producer Organizations), और निजी खरीदारों तक सीधी पहुंच मिलनी चाहिए ताकि वे अपनी फसल को बेहतर दामों पर बेच सकें।
FCI (Food Corporation of India) Annual Report 2024 – खरीद और भंडारण डेटा
MSP पर सरकारी खरीद का सबसे बड़ा हिस्सा FCI (भारतीय खाद्य निगम) करता है। उसकी रिपोर्ट 2024 के मुताबिक:
- खरीद डेटा:
FCI (भारतीय खाद्य निगम) राज्यों से गेहूं और धान की खरीद करता है।- खरीद पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और यूपी में सबसे ज्यादा होती है।
- पूर्वी भारत (बिहार, बंगाल) में खरीद नगण्य रहती है, जिससे वहां MSP का फायदा बहुत कम मिलता है।
- भंडारण:
FCI (भारतीय खाद्य निगम) के गोदामों में बड़ी मात्रा में अनाज रखा जाता है।- 2024 की रिपोर्ट में कुल गेहूं भंडारण, राज्यवार खरीद और वितरण के आंकड़े शामिल हैं।।
- भंडारण चुनौती भी एक बड़ा मुद्दा है – गोदामों की क्षमता, रखरखाव, और अनाज बर्बादी रोकना।
मुख्य बातें (FCI डेटा):
- MSP खरीद की असली कार्यान्वयन एजेंसी
- राज्यवार असमानता – कुछ राज्यों में खरीद मजबूत, कुछ में कमजोर
- भंडारण और वितरण योजना भी MSP नीति का अहम हिस्सा
FCI India Website:
FCI (भारतीय खाद्य निगम) हर साल अपनी वार्षिक रिपोर्ट (Annual Report) और खरीद-भंडारण डेटा वेबसाइट पर सार्वजनिक करता है।
निष्कर्ष – क्यों जरूरी है यह डेटा?
किसी भी MSP सुधार की चर्चा भावनात्मक नारे से नहीं, ठोस सरकारी आंकड़ों और शोध के आधार पर होनी चाहिए।
कृषि मंत्रालय का डेटा बताता है – उत्पादन बढ़ रहा है, MSP घोषित है, लेकिन खरीद सीमित है।
ICAR की स्टडी बताती है – 60% किसानों को MSP का सीधा फायदा नहीं मिलता।
FCI की रिपोर्ट बताती है – खरीद और भंडारण में क्षेत्रीय असमानताएं हैं और सुधार की जरूरत है।
इससे साफ है कि MSP सुधार का मतलब सिर्फ “रेट बढ़ाना” नहीं है – बल्कि खरीद व्यवस्था, केंद्रों की संख्या, डिजिटल भुगतान, मंडी सुधार और भंडारण क्षमता सब सुधारना होगा।
विशेषज्ञों की राय
भारत की न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति और इसके सुधार से जुड़ी चर्चाएं सरकारी घोषणाओं या राजनीतिक वादों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। कई कृषि विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं का मानना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तभी प्रभावी होगा जब इसका ढांचा ज़मीन पर मजबूती से टिका हो।
नीचे तीन प्रमुख स्रोतों – एक कृषि अर्थशास्त्री, एक ICAR वैज्ञानिक और नीति आयोग – की राय को विस्तार से समझाया गया है।
1. डॉ. वी.एस. मिश्रा (कृषि अर्थशास्त्री):
“MSP कानून से किसानों की आय नहीं बढ़ेगी अगर खरीद का सिस्टम दुरुस्त नहीं हो।”
डॉ. मिश्रा कहते हैं कि MSP पर सिर्फ कानून बना देने से किसानों की आमदनी बढ़ना तय नहीं है।
उनकी विस्तार से राय:
- MSP की घोषणा तो केंद्र सरकार हर साल करती ही है।
- लेकिन असली चुनौती है खरीद व्यवस्था – यानी किसानों से फसल खरीदने के लिए पर्याप्त सरकारी केंद्र होना, समय पर भुगतान होना और पारदर्शी प्रक्रिया होना।
- कई राज्यों (जैसे बिहार, बंगाल) में सरकारी खरीद केंद्र बहुत कम हैं। वहाँ किसान व्यापारी को ही बेचने को मजबूर होते हैं, जो MSP से कम दाम देता है।
- अगर MSP को कानूनी गारंटी दे भी दी जाए, लेकिन खरीदने वाला सिस्टम मजबूत न हो, तो किसानों को फायदा नहीं मिलेगा।
- इसके लिए राज्यों में खरीद केंद्रों का जाल, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और डिजिटल पेमेंट जैसी चीजें जरूरी हैं।
सरल शब्दों में:
“कानून से ज्यादा जरूरी है खरीद की मजबूत व्यवस्था – तभी MSP किसानों तक पहुंचेगा।”
2 . डॉ. रंजन कुमार (ICAR विशेषज्ञ):
“फसल विविधीकरण और FPO मॉडल भविष्य है।”
डॉ. रंजन कुमार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) से जुड़े विशेषज्ञ हैं। उनका नजरिया MSP से भी बड़ा है – वे कृषि के भविष्य पर सोचने को कह रहे हैं।
उनकी विस्तार से राय:
- MSP ज्यादातर गेहूं और धान जैसी कुछ फसलों तक सीमित है। इससे देश के कई इलाकों में मोनो-क्रॉपिंग (एक ही फसल बार-बार) बढ़ती है।
- फसल विविधीकरण (Crop Diversification) जरूरी है – मतलब किसान दलहन, तिलहन, सब्जियां, फल और अन्य नकदी फसलों की ओर भी जाएं। इससे बाजार की मांग के हिसाब से उत्पादन होगा और आय बढ़ेगी।
- FPO (Farmer Producer Organization) मॉडल – किसान संगठित होकर उत्पादन बेचें। इससे बिचौलियों की कटौती कम होती है, बड़ी मात्रा में सौदा करने की ताकत बढ़ती है, और प्रोसेसिंग व ब्रांडिंग भी संभव होती है।
- FPO किसानों को बाजार से सीधे जोड़ता है और MSP से भी बेहतर दाम दिला सकता है।
सरल शब्दों में:
“भविष्य सिर्फ MSP पर निर्भर नहीं है – हमें फसल विविधता और FPO जैसे मॉडल पर भी जोर देना होगा।”
3. नीति आयोग (भारत सरकार) – 2024 के सुझाव:

नीति आयोग, भारत सरकार का प्रमुख थिंक-टैंक जो नीति को आकार देने के संबंध में सलाह देता है, नीति आयोगन ने 2024 में एमएसपी में सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण और व्यावहारिक सुझाव दिए हैं।
नीति आयोग के तीन बड़े सुझाव:
1 MSP खरीद टार्गेटेड हो:
- सबके लिए MSP पर खरीदी करना व्यावहारिक नहीं है – भंडारण, बजट और लॉजिस्टिक्स की बड़ी चुनौती होगी।
- सुझाव है कि MSP खरीद उन किसानों या इलाकों में फोकस हो जहां ज्यादा जरूरत है, जैसे छोटे और सीमांत किसान, गरीब राज्य, और ऐसी फसलें जहां बाजार दाम MSP से कम जा रहे हों।
- इससे सरकार की लागत भी नियंत्रित रहेगी और जरूरतमंद किसानों को सीधा फायदा मिलेगा।
2 डिजिटल प्लेटफॉर्म:
- खरीद, भुगतान और लॉजिस्टिक्स की प्रक्रिया पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल सिस्टम जरूरी है।
- ई-नाम जैसे डिजिटल मार्केट प्लेटफॉर्म का समुचित विस्तार किया जाना चाहिए।
- किसान पंजीकरण, खरीदी का आदेश, वजन, गुणवत्ता जांच और भुगतान सब डिजिटल हो ताकि भ्रष्टाचार कम हो और प्रक्रिया तेज हो।
3 एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर:
- MSP खरीद के लिए सिर्फ घोषणा नहीं, ठोस भौतिक ढांचे की जरूरत है।
- गांव-गांव में खरीद केंद्र, मंडियों का आधुनिकीकरण, वेयरहाउस (गोदाम), कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट, और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में निवेश जरूरी है।
- इससे फसल की बर्बादी भी रुकेगी और किसानों को बेहतर दाम मिलेगा।
सरल शब्दों में:
“MSP सुधार का मतलब है – सही जगह फोकस, डिजिटल सिस्टम और मजबूत ढांचा।”
निष्कर्ष – विशेषज्ञों की सम्मिलित राय
MSP को लेकर विशेषज्ञों की राय में कुछ साझा बातें निकलती हैं:
सिर्फ MSP का कानून बना देने से किसानों की आय नहीं बढ़ेगी, जब तक खरीद सिस्टम मजबूत न हो।
फसल विविधीकरण और FPO जैसे सामूहिक मॉडल से किसान बाजार में ताकतवर बन सकते हैं।
नीति आयोग का साफ सुझाव है – MSP सुधार के लिए टार्गेटेड खरीद, डिजिटल प्लेटफॉर्म और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश जरूरी है।
MSP सुधार का मतलब केवल “रेट बढ़ाना” नहीं – बल्कि खरीद, भुगतान, भंडारण, मार्केटिंग और उत्पादन विविधता सबको सुधारना है। तभी किसानों की आय वास्तव में बढ़ेगी और कृषि टिकाऊ बनेगी।
MSP के बिना भविष्य का रोडमैप
भारत में MSP (Minimum Support Price) एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि यह हर किसान तक नहीं पहुंचता। कई राज्यों और फसलों में MSP की खरीदी न के बराबर है। इसलिए जरूरी है कि हम MSP के बाहर भी ऐसी रणनीति बनाएं जिससे किसानों की आय सुरक्षित रहे और उनका भविष्य बेहतर हो।
यह रोडमैप दो हिस्सों में बांटा जा सकता है – अल्पकालीन (Short-term) रणनीति और दीर्घकालीन (Long-term) रणनीति। इसके अलावा, किसानों के लिए कुछ व्यक्तिगत सलाह भी बेहद जरूरी हैं।
1. अल्पकालीन रणनीति – तुरंत लागू करने योग्य कदम
अगले 1 से 2 वर्षों में सरकार और किसान मिलकर ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे न्यूनतम समर्थन मूल्य के अभाव में भी किसानों को बाजार में उनकी उपज का अच्छा मूल्य मिले और उनकी मजबूरी कम हो।
(a) मंडी व्यवस्था को मजबूत करें
- मंडी ही वह जगह है जहां किसान अपनी उपज बेचता है।
- बहुत सी मंडियां पुरानी, भ्रष्टाचारग्रस्त और बिचौलियों के कब्जे में हैं।
- सरकार को मंडियों का आधुनिकीकरण करना चाहिए – जैसे डिजिटल बोली, ई-नाम प्लेटफॉर्म, पारदर्शी वजन और गुणवत्ता जांच।
- इससे MSP न सही, बाजार दर पारदर्शी और उचित मिलेगी।
(b) किसानों को विकल्प दें
- किसानों को सिर्फ स्थानीय व्यापारी पर निर्भर न रहने देना चाहिए।
- राज्य सरकारें और निजी कंपनियां कांट्रैक्ट फार्मिंग, सीधी खरीद, ई-नाम जैसी विकल्प दे सकती हैं।
- किसानों को अपने उत्पाद सीधे रिटेल चेन, प्रोसेसर या निर्यातकों तक बेचने के लिए सपोर्ट चाहिए।
संक्षेप में:
“मंडी मजबूत हो और किसान के पास बेचने के कई विकल्प हों – तभी MSP के बिना भी बेहतर दाम
2. दीर्घकालीन रणनीति – कृषि का मजबूत भविष्य
यह वे कदम हैं जिन्हें 3–10 साल के भीतर बनाना और मजबूत करना होगा ताकि किसान की कमाई स्थायी रूप से बढ़े और बाजार में उसकी स्थिति मजबूत हो जाए।
(a) कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश
- गांव-गांव में वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट बनें।
- इससे फसल खराब नहीं होगी और किसान मजबूरी में सस्ते दाम पर नहीं बेचेगा।
- खरीद केंद्र, गांव मंडी, सड़क और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सुधरें।
(b) वैल्यू एडिशन पर जोर
- किसान कच्चा माल बेचने के बजाय प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बेचे।
- जैसे टमाटर की चटनी, दाल पैकिंग, मसाला ग्राइंडिंग।
- इससे कई गुना ज्यादा दाम मिलता है और रोजगार भी बढ़ता है।
(c) इंटर-स्टेट ट्रेड सुधार
- राज्य सीमाओं के बीच कृषि उत्पाद भेजने में अभी कई टैक्स, परमिट और अड़चनें हैं।
- इन्हें आसान करना चाहिए ताकि किसान देशभर के बाजार में बेच सके और दाम बढ़े।
- किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को दूसरे राज्यों में बेचने के लिए प्रोत्साहन मिले।
(d) फसल बीमा को मजबूत बनाना
- प्राकृतिक आपदा (प्राकृतिक आपदा का अर्थ है, ऐसी घटनाएँ जो प्रकृति के कारण होती हैं और जिनसे जान-माल का भारी नुकसान होता है। ये घटनाएं अचानक हो सकती हैं और गंभीर रूप से मानव जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को प्रभावित कर सकती हैं. ), सूखा, बाढ़ से किसान की फसल तबाह होती है।
- फसल बीमा किसानों के लिए सुरक्षा कवच है।
- बीमा योजना को सरल और पारदर्शी बनाकर किसानों को भरोसा दिलाना होगा।
संक्षेप में:
“दीर्घकालीन में इंफ्रास्ट्रक्चर, वैल्यू एडिशन, ट्रेड सुधार और बीमा से किसान का जोखिम कम होगा और आय बढ़ेगी।”
3. किसानों के लिए व्यावहारिक सलाह
नीचे कुछ ऐसी बातें हैं जो हर किसान को खुद के स्तर पर अपनानी चाहिए, MSP हो या न हो।
(a) अपनी लागत निकालें और न्यूनतम मूल्य तय करें
- किसान अक्सर अपनी लागत का पूरा हिसाब नहीं रखते।
- बीज, खाद, मजदूरी, सिंचाई, ट्रांसपोर्ट – सबका खर्च जोड़कर देखें।
- इससे पता चलेगा कि न्यूनतम कितना दाम लेना जरूरी है।
फायदा:
“व्यापारी से भाव तय करते वक्त मजबूती से बात कर सकते हैं।”
(b) FPO से जुड़ें
- अकेले किसान की बाजार में ताकत कम होती है।
- FPO (Farmer Producer Organization) में दर्जनों-सैकड़ों किसान मिलकर एक संगठन बनाते हैं।
- सामूहिक बिक्री, थोक खरीद, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग – सब आसान हो जाता है।
- MSP से भी अच्छा भाव मिलने की संभावना बढ़ती है।
फायदा:
“एकता में ताकत – मिलकर बेचें, बेहतर दाम पाएं।”
(c) मार्केट जानकारी लें
- आज के जमाने में बाजार की मांग और दाम जानना जरूरी है।
- इंटरनेट, मंडी भाव ऐप, रेडियो, कृषि विभाग से जानकारी लें।
- कौन सी फसल ज्यादा बिक रही है, कहाँ दाम अच्छा है – यह जानकर वही फसल लगाएं।
फायदा:
“बाजार के हिसाब से प्लानिंग करके घाटा रोकें।”
निष्कर्ष – MSP के बिना भी सुरक्षित और बेहतर खेती संभव है
MSP एक जरूरी नीति है लेकिन इसका कवरेज सीमित है। इसलिए सरकार और किसानों को दोनों स्तर पर काम करना होगा:
✔ अल्पकालीन – मंडियां ठीक करें, किसान को विकल्प दें
✔ दीर्घकालीन – इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेसिंग, बीमा, और ट्रेड को सुधारे
✔ किसान – अपनी लागत समझे, संगठित हो, और बाजार को जाने
ऐसा करके MSP के बिना भी किसान की आय सुरक्षित और मजबूत हो सकती है, और भारतीय कृषि का भविष्य ज्यादा टिकाऊ और लाभकारी बन सकता है।
निष्कर्ष
2025 में MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) किसानों के लिए एक बहस नहीं, बल्कि एक जमीनी चुनौती बन गया है। MSP की घोषणा तो होती है, लेकिन हकीकत यह है कि बहुत सारे किसानों को इसका वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। कारण है – खरीद की कमजोर व्यवस्था, मंडी में पारदर्शिता की कमी, और सीमित पहुंच।
इसलिए सवाल यह नहीं कि “MSP गारंटी का कानून बने या नहीं”, बल्कि यह है कि किसानों को आय कैसे सुनिश्चित हो? MSP तभी कारगर होगी जब साथ में संपूर्ण सिस्टम में सुधार होगा।
MSP का गणित – 2025 की स्थिति
- भारत सरकार ने गेहूं, धान, दाल, तिलहन आदि के लिए MSP घोषित किया है।
- लेकिन सरकारी खरीदी महज 25-30% फसलों तक सीमित है।
- बाकी किसान प्राइवेट व्यापारियों को बेचने को मजबूर हैं, जहाँ MSP का कोई मूल्य नहीं।
- कई राज्यों (जैसे बिहार, ओडिशा, बंगाल) में खरीद केंद्र या तो नहीं हैं, या काम नहीं कर रहे।
इसलिए MSP की घोषणा, बिना मजबूत सिस्टम के, सिर्फ कागज़ी भरोसा बनकर रह जाती है।
समाधान सिर्फ MSP कानून नहीं – ज़मीनी सुधार हैं
किसानों को ज़रूरत है विकल्पों की
किसान को सिर्फ एक मंडी या व्यापारी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्हें अपनी फसल बेचने के अलग–अलग रास्ते मिलें – जैसे:
- डिजिटल मंडी (e-NAM)
- किसान उत्पादक संगठन (FPO)
- सीधी बिक्री (Direct Buyer)
- प्रोसेसिंग यूनिट या रिटेल चेन
ज्यादा विकल्प = बेहतर दाम और सुरक्षित आय
MSP से ज्यादा जरूरी चार ज़मीनी चीजें:
1. खरीद केंद्रों का विस्तार
- MSP तभी असरदार है जब सरकार फसल खरीदे
- हर गांव/ब्लॉक स्तर पर खरीद केंद्र खोलना जरूरी है
- मोबाइल खरीद केंद्र (चलती गाड़ियां) भी ग्रामीण इलाकों में उपयोगी हो सकते हैं
बिना खरीदी, MSP सिर्फ एक पोस्टर बन जाती है।
2. पारदर्शी मंडी व्यवस्था
- मंडियों में बोली और दाम तय करने की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार आम बात है
- बोली पारदर्शी हो, इलेक्ट्रॉनिक तौल हो, रेट लिस्ट डिस्प्ले हो – तभी किसान को न्याय मिलेगा
- दलालों और बिचौलियों की भूमिका सीमित करनी होगी
MSP पारदर्शिता के बिना अधूरी है।
3. डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म
- यदि किसानों को खरीद के लिए ई-नाम, कृषि बाजार या राज्य पोर्टल जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीधे जोड़ा जाए तो उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी अधिक कीमत मिल सकती है।
- डिजिटल रजिस्ट्रेशन, मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की प्रक्रिया आसान बनाई जाए
तकनीक से बाजार में किसान की हिस्सेदारी मजबूत होती है।
4. FPO नेटवर्क को मज़बूत करना
- अकेले किसान की मोल-भाव की ताकत कम होती है
- एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) किसानों को एक साथ संगठित करता है और उन्हें बड़े पैमाने पर बिक्री, ब्रांडिंग, प्रसंस्करण और उचित लेन-देन करने के लिए सशक्त बनाता है।
- MSP की गैर-मौजूदगी में FPO सबसे अच्छा विकल्प बन सकता है
FPO = किसान की बाज़ार में एकजुट शक्ति
समझदारी क्या कहती है?
MSP की मांग जायज़ है, लेकिन उसका असर तभी होगा जब:
✔ सरकार खरीदी करे
✔ सिस्टम पारदर्शी हो
✔ तकनीक और मार्केटिंग से किसान सशक्त हो
✔ FPO मॉडल को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूत किया जाए
अंतिम शब्द:
“किसान को सिर्फ दाम नहीं – व्यवस्था चाहिए
MSP सिर्फ घोषणा नहीं – सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए
और सबसे जरूरी – किसान को विकल्प और ताकत दोनों मिलने चाहिए”
अगर आपको यह लेख पसंद आया, तो शेयर करें
अपने अनुभव नीचे कमेंट में बताएं
किसान भाईयों के लिए ऐसी और गाइड पढ़ें
[किसान क्रेडिट कार्ड रुपये 5 लाख तक—डॉक्यूमेंट लूपहोल्स से कैसे बचें?]
